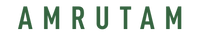Read time : min
आयुर्वेदिक चिकित्सा की लोकप्रियता देश में ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ रही है। आज आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति जन साधारण में विश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति कही जा सकती है।
आयुर्वेद में फूल, पत्ती, वृक्षों तथा स्पर्श तक की चिकित्सा के उपाय सुझाये गये हैं।
आयुर्वेद की इस विलक्षण चिकित्सा पद्धति का विकास किस तरह हुआ! प्रस्तुत है जानकारियों से भरा यह ज्ञानवर्धक विवरण!
प्रथ्वी पर अवतरण के साथ ही मनुष्य को व्याधियों का अभिशाप मिला। जन्म से अंत तक हरेक को रोगों भय सताता रहता है।
सबसे बड़ी व्याधि है...मृत्यु।
सतयुग से ही मनुष्य ने स्वयं को अमर बनाने की चेष्टा की और उसकी यह चेष्टा आज भी इतनी ही जागरूक है, जितनी पहले किसी समय थी।
समुद्र मंथन से निकला अमृत भी विवाद
का कारण बना। क्योंकि देव या दैत्य दोनों
ही अमर होना चाहते थे। इस प्रक्रिया में दैत्यों
और राहु के साथ धोखा हुआ।
देवता या राक्षसों एवं ऋषि, महर्षियों ने
भी रोगों से मुक्त होने या युद्ध करने के
अनेक उपाय किये गये और उन रोगों के
कारणों को समझने का प्रयत्न किया गया।
हम यह तो नहीं कह सकते कि इस प्रयास
के कारण रोग लुप्त हो गये या उनकी भयंकरता
कम हो गयी।
परंतु इतना तो स्पष्ट है कि देह को दुरुस्त
रखने के इस प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य
ने अनेक आविष्कार और प्रयोग किये तथा
उसने प्राकृतिक पदार्थों का निरीक्षण प्रारंभ किया।
दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में उपलब्ध खनिजों,
जंतुओं एवं वनस्पतियों का निरीक्षण तथा
विश्लेषण किया गया और पारस्परिक
सम्मिश्रण से अनेक योग या फार्मूले
(यौगिक तथा मिश्रण) तैयार किये
गये, जिनके आधार पर किसी-न-
किसी रोग को दूर करना संभव
माना गया।
समाज के ऐश्वर्य की जैसे-जैसे
अभिवृद्धि हुई, उसका घात-प्रतिघात
मनुष्य के शरीर के साथ भी हुआ।
कुछ रोगों का शमन हुआ, तो उस शमन के साथ-साथ कुछ अन्य रोगों का प्रादुर्भाव हुआ और यह क्रम आज तक निरंतर चला आ रहा है।
अमर बनने की अभिलाषा ....
जरा और मृत्यु से मुक्त होकर अमर बनने की मानव की सुप्त आशा के फलस्वरूप ही आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं विकास हुआ।
आयुर्वेदके आदि देवता भगवान शिव हैं जिन्हें बाबा वैद्यनाथ भी कहते हैं।
वेद का एक मंत्र है जिसका अर्थ है, “हे वेधनाथ महादेव! जब आप प्रेरणा देते हैं तो आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मानवी औषधियां उत्पन्न होती हैं।"
समुद्र मंथन के फलस्वरूप अमृत-कलश के साथ भगवान धन्वन्तरि समुद्र से प्रकट हुए थे। उस अमृत का निर्माण भगवान भोलेनाथ ने ही किया था।
चरकसंहिता (सूत्रस्थान प्रथम अध्याय) में आयुर्वेद परंपरा का एक अन्य विवरण है। इसमें लिखा है कि महादेव ने ब्रह्माजी की तपस्या से प्रसन्न होकर आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्माजी ने इसका प्रचार आगे बढ़ाया।उन्हें इस आयुर्वेद-शास्त्र के प्रथम प्रवर्तक या प्रचारक बताया है।
ब्रह्मा से यह ज्ञान प्रजापति (दक्ष) ने सीखा, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और अश्विनी कुमारों से इंद्र ने सीखा।
सप्तऋषियों ने जड़ीबुतियों की खोज कर
अनेक ग्रंथ लिखे...
तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों में 'रोग विघ्न डालने लगे, तो हिमालय के पार्श्व में महर्षियों का सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेनेवाले महर्षियों के नामों की लंबी सूची भी दी है। इनमें प्रमुख थे .....अंगिरा, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भृगु, गौतम, पुलस्त्य, नारद, भारद्वाज, विश्वामित्र, च्यवन, अगस्त्य, मारीच, धौम्य आदि ।
पर्यावरण के इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महर्षि भारद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इंद्र के पास जाए।
इंद्र ने भारद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश दिया
और हेतु, शिवलिंग तथा औषध, इस त्रिशूल का
ज्ञान कराया। ज्ञान-दान की यह परंपरा आगे बढ़ी
और महर्षि पुर्नवसु तक पहुंची।
सब प्राणियों पर अनुकंपा करके पुनर्वसु ने यह आयुर्वेद-ज्ञान अपने छह शिष्यों को दिया।
ये शिष्य अग्निवेश, भेल, पराशर, जतूकर्ण,
हारीत और क्षारपाणि थे।
पुनर्वसु और उनके छह शिष्य अथर्ववेद की ऋषि-नामावलि में स्थान नहीं पाते हैं।
अतः, यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद की परंपरा, वैदिक-काल से अब आगे की ओर बढ़ी। पुनर्वसु के सब शिष्यों में अग्निवेश विशेष प्रतिभाशाली थे और वे ही
आयुर्वेद-ज्ञान के प्रथम संकलनकर्ता माने गये।
अन्य भेल आदि शिष्यों ने भी संकलन किया और सबने अपने-अपने संकलन एक ऋषि-परिषद् में सुनाये, जिसके सभापति आत्रेय थे।
इस परिषद् में जो कुछ भी संकलन किया गया, वह चरक द्वारा फिर से संपादित और संशोधित होकर, हमारे सामने 'चरकसंहिता' के रूप में उपस्थित हुआ।
चरक कौन थे? ....वस्तुतः, अग्निवेश ही चरक थे। चरकसंहिता के रचयिता अग्निवेश ही थे, जैसा कि प्रत्येक अध्याय के अंत में इस ग्रंथ में स्वयं निर्दिष्ट है-“इत्यग्निवेशकृते...."।
आयुर्वेद की इस नयी परंपस में 'पुनर्वसु' सबसे महान आविष्कारक हुए और अग्निवेश (चरक) सबसे बड़े संपादक-संशोधक।
पुनर्वसु ने एरंड (अरंडी, रेंडी) तेल के विरेचन में सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो आज तक चिकित्सा-शास्त्र में समस्त संसार में प्रचलित है।
अथर्ववेद : चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता....
चारों वेदों में एक अथर्ववेद, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता है इसे 'आंगिरस' या 'त्रिषग्वेद' भी कहते हैं।
अथर्ववेद में सभी रोगों के लक्षण तथा औषधियों का विस्तार से उल्लेख है।
अथर्ववेद से आयुर्वेद-शास्त्र ने प्रथम प्रेरणा पायी। अपामार्ग, पिप्पली और अरुन्धती-ये तीन सर्वप्रथम वनस्पतियां हैं, जिनका उपयोग व्याधियों और कष्टों के निवारण करने में मनुष्य ने आदिमकाल में सीखा।
चरक संहिता का दूसरा अध्याय
इस वाक्य से आरंभ होता है।
“अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलीमरिचानि च।"
(सू. २/३)।
इस बात से ही अपामार्ग और पिप्पली की, जिसका विशद उल्लेख अथर्ववेद में है, प्रधानता का अनुमान हो सकता है। साथ ही, इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि वनस्पति-औषधों की परंपरा भी अथर्ववेद में वर्णित अपामार्ग और पिप्पली से ही शुरू हुई। -
आयुर्वेद के प्रथम गुरु पशु थे....
मनुष्य ने औषधशास्त्र कहां से सीखा?
कैसे उसने जाना कि अमुक-अमुक वनस्पतियां
हमारे काम की हैं?
इस संबंध में मनुष्य ने पशुओं को अपना
गुरु बनाया। उसने देखा कि पशुओं में एक
प्राकृतिक प्रेरणा होती हैं, जिससे कष्ट के समय
वे अपने चारों ओर उपलब्ध वनस्पतियों में से किन्हीं का सेवन करते हैं।
बिना झोली के फकीर लेकिन
ज्ञानी होते हैं - पशु....
पशुओं के सहारे आविष्कार करने की प्रेरणा मनुष्य ने अथर्ववेद के तीन मंत्रों (अथर्व, ८/७/२३-२५) से प्राप्त की, जिनका हिंदी अनुवाद है:
"कुछ पौधों को वराह (सूअर) जानता है और
कुछ औषधियों को नेवला तथा
कुछ को सांप और गंधर्व।
कुछ अंगिरसी औषधियां सुपर्ण (चील, गिद्ध)
जानते हैं और कुछ को रांघट जानता है।
कुछ को वयस् (पक्षी) तथा अन्य सब पतत्री (पंखवाली चिड़िया) जानते हैं।
कुछ औषधियों को मृग जानते हैं।
उनमें से कुछ का मैं आवाहन करता हूं।
न जाने कितनी औषधियां गायें चरती हैं और
कितनी भेड़ें तथा बकरियां।
ये सभी औषधियां!
तुम्हारे लिए लायी जाएं तथा सभी के लिए कल्याणकारी एवं पोषक हों।"
आयुर्वेद के आचार्य तुल्यगुणों के आधार पर
बहुत-सी औषधियों के आविष्कार की ओर अग्रसर हुए।
रक्तशोधक औषधियों की खोज...
अगर कोई चीज लाल है और घुलने पर लाल रंग का विलयन देती है, तो वे अपनी खोज को इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ाते थे कि यह रक्तशोधक हो सकती है और रक्त-स्राव से भी रक्षा कर सकती है।
वीर्यवर्धक औषधियों की खोज केसे हुई...
यदि कोई चीज दूध के समान श्वेत और गाढ़ी है,
तो यह वीर्यवर्द्धक और ओजप्रद हो सकती है।
इस प्रकार के सादृश्यों के आधार पर भी कुछ औषधियों का आविष्कार हुआ।
महर्षि आत्रेय पुनर्वसु....
पुनर्वसु का पूरा नाम आत्रेय पुनर्वसु था।
चरक संहिता में कई ऐसे विचार-विमर्शों
(गोष्ठियों) का उल्लेख आता है, जो आत्रेय
पुनर्वसु के सभापतित्व में हुए। आत्रेय ने विचार-स्वतंत्रता और विचार-विनिमय पर बड़ा बल दिया है।
चरक संहिता के विमान स्थान के आठवें अध्याय में विचार-विनिमय (जिसे संभाषा कहा गया है) के विस्तृत नियम दिये हुए हैं।
'त्रिषगू त्रिग्वजासह संभाषेत' अर्थात वैद्य के साथ वैद्य संभाषण करे, क्योंकि विचार-विनिमय स्पर्धा करनेवाला होता है और निर्मलता लाता है।
वैद्य, भगवान शिव का उपासक हो।
वह, वचन-शक्ति को उत्पत्र करता है और यश को बढ़ाता है। वह शास्त्र-संदेह को दूर करता है और निश्चय को उपलब्ध कराता है।
आत्रेय पुनर्वसु के आविष्कारों और उपदेशा को अग्निवेश (चरक) ने विस्तार से लिखा और उन्हें क्रमबद्ध किया।
अग्निवेश ने जो रूप दिया, वही आज चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। आत्रेय के 'चिकित्सा शास्त्र' को भी अग्निवेश ने इसी प्रकार लिखा।
चरक संहिता लाखों वर्ष पुराना ग्रन्थ है....:
चरक संहिता हमारे आर्य-साहित्य का अति प्राचीन वैद्यक ग्रंथ है । प्राचीन अरब देश के लेखक भी इसका उल्लेख करते हैं।
संपूर्ण चरक संहिता का अरबी में अनुवाद भी हुआ, जैसा कि अलबेरूनी के प्रमाण से स्पष्ट है।
तिब्बती और चीनी भाषाओं के आयुर्वेद-साहित्य पर भी इस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा। अलबेरूनी ने लिखा है, "हिंदुओं की एक पुस्तक है, जो लेखक के नाम पर 'चरक' , प्रसिद्ध है।
यह औषध-विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है।" किंवदंती यह है कि चरक ऋषि द्वापर में हुए और उनका नाम अग्निवेश था।
बुद्धिमान होने के कारण वे 'चरक' कहलाये। चरक संहिता से ही पता लगता है कि चरक के समय बाहलीक, पहलव, चीन, शूलीक, यवन और शक भारत में आने-जाने लगे थे
दुर्लभ आयुर्वेदिक वनस्पतियों की सुरक्षा
"बाहनीका: पहलवाश्चीनाः शूलीकाः यवनाः शका:" (चरक. चि. ३०/३१६)। साथ ही, चरक को इन देशों के निवासियों के आहार-विहार और स्वभाव का पता था।
चरक संहिता के ४३ के लगभग पुरानी टीकाएं पायी जाती हैं। चरक के टीकाकारों में भट्टार हरिचंद्र, स्वामिकुमार, शिवदास सेन, जेज्जट और चक्रपाणि बहुत प्रसिद्ध हैं।
भारत में प्रत्येक युग में आयुर्वेद की परंपरा रही है। न जाने कितने एकांगी या सर्वांगी ग्रंथ लिखे गये, कितने ही ग्रंथों की टीकाएं लिखी गयीं और इनमें से बहुत-से ग्रंथ क्षणजीवी ही रहे।
ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में आयुर्वेद के ग्रंथों की एक नामावली है, जिसका उल्लेख अन्य आयुर्वेद - ग्रंथों में भी यत्र-वत्त है, पर ये ग्रंथ अब पाये नहीं जाते।
शल्य चिकित्सा का प्रादुर्भाव औषध-चिकित्सा की भांति शल्य चिकित्सा का प्रादुर्भाव भी अथर्ववेद की ही प्रेरणा से हुआ। इसके प्रवर्तक सुश्रुत हुए।
चरक के समान सुश्रुत भी अति प्राचीन हैं।
महाभारत में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है। चरक के समान सुश्रुत की कीर्ति भी भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गयी थी।
पूर्व में कम्बोडिया तक, पश्चिम में अरब तक इनका यश पहुंच चुका था। 'सुश्रुतसंहिता' में पहला सूत्रस्थान है जिसमें लिखा है कि काशी नरेश दिवोदास (जो धन्वन्तरि के अवतार थे), सुश्रुत के गुरु थे।
सुश्रुत संहिता : आज भी वरदान शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में तो सुश्रुत संहिता इस युग के लिए भी वरदान है। इसमें शल्य-चिकित्सा के सभी पहलुओं को अत्यंत विस्तार एवं सूक्ष्मता से समझाया गया है।
सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि जब शिष्य सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाए, तब उसे स्नेहकर्म (ओलिएशन) और छेद्यकर्म (ऍम्पुटेशन) का उपदेश देना चाहिए।
छेदयकर्म सिखाने के लिए काशीफल, लौकी, तरबूज, खरबूजा, फूट, पेठा, ककड़ी आदि के समान फलों का आश्रय लेना चाहिए। इन फलों में उत्कर्तन (ऊपर काटना) और अपकर्तन (नीचे काटना) सिखाना चाहिए। मशक या चमड़े आदि के थैले में पानी या कीचड़ भरकर भेद्यकर्म (इन्सीजन्स) सिखाना चाहिए।
खुरचने का काम किसी तने हुए चमड़े पर, जिस पर बाल भी हों, सिखाना चाहिए।
वेध्यकर्म (वेनिसेक्शन) के लिए मृतपशु का शिरा या कमलनाल लेकर सिखाना चाहिए। इसी तरह, शल्य-क्रिया के विभिन्न अंगों को सिखाने की सैकड़ों विधियां सुश्रुत संहिता में दी हुई हैं।
भारी संख्या में शल्य चिकित्सा संबंधी मंत्रों की रचना एवं प्रयोग विधि इस पुस्तक में विस्तार से समझायी गयी है।
शल्यकर्म का विशेष उपयोग युद्ध में आहत सैनिकों के लिए आरंभ हुआ था। प्रत्येक राजा - अपने साथ औषध-चिकित्सक और शल्यकर्मनिपुण वैद्य रखता था।
सुश्रुत संहिता एक पूरा अध्याय 'युक्तसेनीय' नाम का है, जसमें सेना के संबंध में शल्यकर्म का विधान।
राजा जब शत्रु पर विजय प्राप्त करने की च्छा से सेना लेकर चले, तो राजवैद्य कैसे सकी रक्षा करे, इसका यहां वर्णन है।
सड़कों, पानी, छाया, भोजन और ईंधन को शत्रु दूषित देते हैं। अतः, राजवैद्य का कर्त्तव्य है कि इन दूषणों का पता लगाये और इनका शोधन करे।
रसमंत्रविशारद वैद्य का कर्त्तव्य है कि वह राजा को भावी रोग और मृत्यु से रक्षा करे।
सुश्रुतसंहिता में निर्देश है कि राजा के शिविर के बाद ही सभी उपकरणों से संपन्न होकर राजवैद्य एक तंबू में रहे। उसके तंबू पर एक झंडा लटकता हो, जिससे विष, घाव और रोग से पीड़ित व्यक्ति बिना कठिनाई के वहां जा सके।
वृक्षों की चिकित्सा....
प्राचीन भारतीय ग्रंथों (वृहत्संहिता अध्याय ५४, अग्निपुराण अध्याय २८१) में वृक्षायुर्वेद के अंतर्गत वृक्षों के रोगों की चिकित्सा उसी प्रकार दी है, जैसे मनुष्य के रोगों की चिकित्सा।
शंकर मिश्र ने वैशेषिक की उपात्कर टीका में पौधों के संबंध में 'भेषजप्रयोग' का वर्णन किया है (४/२/५)। वराहमिहिर ने पौधों के रोगों के कारणों की मीमांसा की है।
लज्जावती (छुई-मुई) के लज्जालु होने के कारणों का उल्लेख 'गुणरत्न' ने किया। इन्होंने ऐसे पौधों एवं वृक्षों की सूची भी दी है, जो सोते और जागते हैं।
'सार-संक्षेप
- अथर्ववेद में वृक्षों के चैतन्य होने के संबंध में अनेक तर्क दिये गये हैं-गरमी से इसके पत्तों को झुलसना आदि त्वक्शक्ति का बताता है।
वायु, अग्नि और विद्युत के घोष (शब्द) का इन पर प्रभाव, इनकी श्रवण-शक्ति का सूचक है।
गंध, धूप द्वारा इनके रोगों का निवारण होना और फिर से पुष्पित हो उठना, इनमें घ्राणशक्ति होना बताता है।
मूलों द्वारा रस का पान करना, रसनाशक्ति को द्योतक है। काटे जाने पर और विरोहण पर सुख-दुख भी इनमें होता है।
लता, वृक्ष के शरीर को लपेटती चलती है, अतः, इनमें नेत्र की भी शक्ति है।
चरक के कल्पस्थान के मदनकल्प संबंधी प्रथम अध्याय में लिखा है कि पौधों का औषधीय प्रभाव देश-काल आदि पर निर्भर है।
इसी अध्याय में चरक ने वत्सक पौधों के संबंध में लिंगभेद (स्त्री-पुरुष का भेद) भी दिया है।
जिस वत्सक के फल बड़े हों, फूल सफेद हों और पत्ते चिकने हों, वह नर वत्सक है तथा जिसके फूल श्याम या अरुण हों एवं जिसके फल और डंठल छोटे हों, वह नारी वत्सक है।
केतकी के संबंध में, सितकेतकी को नर और स्वर्ण केतकी को नारी माना गया है।
स्वर्णकेतकी को कनकप्रसवा और सुगन्धिनी बताया गया है।
मानव-स्वास्थ्य पर वृक्षों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विशद वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में है।
वर्तमान विज्ञान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वस्तुतः, इस समय यह शोध का एक महत्त्वपूर्ण विषय है।
मंगलकारी वृक्ष....
वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' के वृक्षायुर्वेदाध्याय (अ.५४) में लिखा है कि घर और बगीचों में अरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, शिरीष और प्रियंगु का लगाया जाना मंगलकारी है।
काश्यप (कश्यप नहीं) ने देवालय, उद्यान, गृह, और उपवन में चंपक, उदुम्बर और पारिजातक का लगाया जाना स्वास्थ्यवर्द्धक बताया है।
अग्निपुराण में उत्तर की ओर प्लक्ष, पूर्व की ओर वट, दक्षिण की ओर आम और पश्चिम की ओर अश्वत्थ लगाने की सम्पति दी है।
कंटकद्रुम मकान के दक्षिण की ओर लगाना अच्छा बताया है। अन्य वृक्ष, जो लगाने के लिए बताये गये हैं, वे हैं-अरिष्टाशोक, पुत्राग, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली, जम्बु, बकुल और दाडिम।
नक्षत्र और वृक्ष...
किस वृक्ष को किस माह में, किस नक्षत्र में और किस ऋतु में लगाया जाए, इसके विवरण हर वृक्ष के लिए अलग-अलग दिये हुए हैं।
डाली काटकर लगाने (कण्डारोपण) से कलम लगाना श्रेष्ठ बताया गया है और इसमें अलग-अलग वृक्ष के लिए अलग-अलग विधि बतायी गयी है।
वृहत्संहिता में बताया गया है कि वृक्ष २० हाथ से १२ हाथ तक की दूरी पर लगाने चाहिए। अधिक पास लगे वृक्ष अस्वस्थ रहते हैं और ठीक से नहीं फलते हैं।
नरम जमीन, जिसमें तिल बोया गया हो और तिल के फूलने पर ही जो जोत डाली गयी हो, आरोपण के कार्य के लिए अच्छी होती है। कितना सूक्ष्म अध्ययन है !
वृहत्संहिता (अध्याय ५४) और अग्निपुराण (अध्याय २८१) में वृक्षायुर्वेद नाम से एक पूरा अध्याय है, जिसमें पेड़ और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए खाद का विस्तृत वर्णन है।
खाद की जानकारी...
यदि फल-फूलों की वृद्धि करनी हो, तो घी, ठंडे दूध, तिल, बकरी और भेड़ का विष्टा तथा
यवचूर्ण- इनके मिश्रण को सात रात सड़ाकर पौधों में डालना चाहिए।
मछली के धोवन के पानी के प्रयोग से पौधों में पत्ते अच्छे निकलते हैं।
आम के लिए, अग्निपुराण में मछली का • ठंडा पानी श्रेयस्कर बताया गया है --
"मत्स्योदकेन शीतेन आम्रणां सेक इष्यते।"
आम के संबंध में, यह प्रथा बंगाल के बागों में आज भी बरती जाती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए खाद बनाने की बहुत सारी विधियां दी हुई हैं जिन्हें बागवानी तथा कृषि से जुड़े लोग अपने घर में ही सरलता से तैयार कर सकते हैं। बस, उन्हें बताने की जरूरत है — विस्तृत अध्ययन के बाद।
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति
भारत की आयुर्वेद पद्धति और यूनान की चिकित्सा पद्धति में इतनी अधिक समानता है कि यह जानने की सहज इच्छा होती है कि क्या आयुर्वेद की भांति यूनानी प्रणाली का उद्भव भी अथर्ववेद की ही प्रेरणा से हुआ।
भारतीय आयुर्वेद का संबंध न केवल यूनान से है, बल्कि अरब, चीन, तिब्बत, फारस एवं अन्य देशों से भी है।
वात-कफ-पित्त का त्रिदोष सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑव ह्यूमर्स) दोनों देशों के आयुर्वेद में पाया जाता है।
वात-कफ-पित्त के समन्वय में न रहने से ही रोग उत्पन्न होते हैं ऐसी मान्यता दोनों देशों में है। कुछ महत्त्वपूर्ण समानताएं इस प्रकार हैं-
(१) ज्वर और अन्य व्याधियों की तीन स्थितियां यूनानी त्रय ग्रीक शब्द (अपेसिया, पेसिस और क्राइसिस) से सूचित होती है; चरकसंहिता में भी ज्वर का पूर्व रूप, ज्वर का अधिष्ठान और ज्वर की प्रत्यात्मिक स्थिति, ये तीन ही हैं।
(२) रोग का शमन जिन विधियों से होता है, उन्हें भारतीय और यूनानी दोनों पद्धतियों में 'शीत-उष्ण' एवं ‘शुष्क-स्निग्ध' विभागों में बांटा गया है।
(३) विरोधी प्रवृत्तिवाले उपायों से रोगों का शमन होता है, ऐसा दोनों मानते हैं।
(४) यूनानी और भारतीय, दोनों के रोग-लक्षण परीक्षण (प्रॉगनोसिस) की विधि एक-सी है।
(५) वैद्यों और शल्यचिकित्सकों को शपथ लेनी होती है और उनके लिए जो आचार-नियम हैं, वे दोनों में शत-प्रतिशत समान हैं।
(६) यह दोनों मानते हैं कि स्वास्थ्य पर ऋतुओं का प्रभाव है।
(७) दैनिक (क्वाटिडियन), तृतीयक (टेशियरी) और चतुर्थक (क्वार्टन) ज्वरों का दोनों में एक-सा उल्लेख है।
(८) दोनों में क्षयरोग का एक जैसा उल्लेख है और उसे बहुत महत्त्व दिया गया है, यद्यपि हृदय-रोग का विशेष वर्णन नहीं है।
(९) गर्भ-स्थिति के भी दोनों शास्त्रों में एक-से वर्णन हैं। दोनों में जुड़वां बच्चे, बच्चे होने और समागम की एक-सी विधियों के उल्लेख हैं।
दोनों यह मानते हैं कि आठवें माह में गर्भ में ओज आता है। न कि सातवें महीने में।
मृत भ्रूण के निकालने में भी समानता है।
(१०) शल्य-कर्म भी दोनों के एक-से हैं।
(११) भेदन-छेदन के प्रयोग भी दोनों में एक-से हैं। (१२) शल्य यंत्रों में भी समानता है।
इनके अतिरिक्त, अन्य अनेक समानताएं भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति और यूनानी चिकित्सा-विधि में हैं। हो सकता है कि दोनों देशों में स्वतंत्र रूप से एक-सा विकास हुआ हो।
त्रिदोष का सिद्धांत क्या है?..
ऐसा लगता है कि त्रिदोष का सिद्धांत, यूनान ने भारतीय आयुर्वेद से लिया। उपरोक्त त्रिदोषवाद के सिद्धांत का विकास, सांख्य के सत्व, रजस् और तमस् जैसे त्रिगुणों के समान, भारत में ही हुआ (अथर्ववेद में इस पर एक पूरा सूक्त है)।
यूनानियों ने भारत की अनेक औषधों को अपनाया और अपने अस्थिज्ञान तथा शल्य-ज्ञान को भी, भारतीय आधार पर, विकसित किया।
आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई, लेकिन यूनानी चिकित्सा प्रणाली का आविर्भाव अथर्ववेद से हुआ अथवा नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है।
जाने...ओषधि, औषध या औषधि में फर्क...
वे वनस्पतियां ओषधि कहलाती हैं, जो एक बार फल- बीज देकर मर जाती हैं (ओषध्य : फलपाकांतः)।
जो ओषधि से तैयार किया जाए, वह औषध।
आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग की जानेवाली वनस्पतियों एवं जड़ी-बूटियों को यदि हम ओषधि कहें, तो उनसे तैयार योग (काढ़ा, क्काथ आदि) को हम औषध कहेंगे।
संस्कृत की दृष्टि से औषधि शब्द अशुद्ध है।
अमृतम दवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सर्च करें..
अमृतम उत्पादों के अपने क्षेत्र में डीलर शिप हेतु संपर्क करें..,9926456869 दीपक